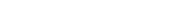Table of Contents
भारत में मृदा के प्रकार भाग -3
मृदा चट्टान के मलबे एवं कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण है जो पृथ्वी की सतह पर विकसित होते हैं। यद्यपि, संपूर्ण मृदा एक समान नहीं है एवं इसके घटकों में विविधता पाई जाती है। पिछले लेख में, हमने मृदा की विभिन्न परतों पर चर्चा की है। पहले लेख में हमने जलोढ़ मृदा एवं काली मृदा पर चर्चा की। दूसरे लेख में, हमने लाल मृदा, लैटेराइट मृदा तथा पर्वतीय/वन मृदा पर चर्चा की। इस लेख में, हम शुष्क या रेगिस्तानी मृदा, लवणीय तथा क्षारीय मृदा एवं पीट, तथा कच्छ भूमि मृदा / दलदली मृदा पर चर्चा करेंगे।
शुष्क या रेगिस्तानी मृदा
- अधिकांश रेगिस्तानी मृदा में वायूढ़ (एओलियन) रेत-पवनों के प्रभाव में रेगिस्तानी रेत- (90 से 95 प्रतिशत) एवं मृदा (5 से 10 प्रतिशत) होती है।
- शुष्क मृदा लाल से भूरे रंग की होती है।
- कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा इतनी अधिक होती है कि खारे पानी को वाष्पित करके सामान्य नमक प्राप्त किया जाता है।
- शुष्क जलवायु, उच्च तापमान एवं त्वरित वाष्पीकरण के कारण इनमें नमी तथा ह्यूमस की कमी होती है।
- मृदा की उपस्थिति से मृदा की वृद्धि बाधित होती है। कैल्शियम की मात्रा नीचे की ओर बढ़ने के कारण मृदा के निचले संस्तर पर कंकड़ की परतें अध्यासित हो जाती हैं।
- निम्न संस्तरों में ‘कंकर’ परत का निर्माण जल के अंतः स्यंदन को प्रतिबंधित करता है एवं इस प्रकार जब सिंचाई उपलब्ध कराई जाती है, तो पौधों की स्थायी वृद्धि के लिए मृदा की नमी आसानी से उपलब्ध होती है।
शुष्क मृदा का वितरण
- रेगिस्तानी मृदा पश्चिमी राजस्थान, कच्छ के रण, दक्षिण हरियाणा एवं दक्षिण पंजाब की पट्टी में पाई जाती है।
- ओडिशा, तमिलनाडु तथा केरल के तटीय क्षेत्रों में, मृत्तिका के बिना रेतीली मृदा भी आम है।
शुष्क मृदा के रासायनिक गुण
- ये मृदा खराब होती हैं तथा इनमें ह्यूमस एवं कार्बनिक पदार्थ अत्यंत कम मात्रा में होते हैं।
- इस मृदा में नाइट्रोजन अपर्याप्त होती है तथा फॉस्फेट की मात्रा सामान्य होती है।
- कुछ रेगिस्तानी मृदा कैल्शियम कार्बोनेट जैसे घुलनशील लवणों की अलग-अलग मात्रा के साथ क्षारीय होती हैं।
शुष्क मृदा की फसलें
- फॉस्फेट तथा नाइट्रेट जहाँ भी नमी उपलब्ध हो, शुष्क मृदा को उपजाऊ बनाते हैं।
- पर्याप्त सिंचाई प्रदान करके मृदा का सुधार किया जा सकता है।
- इस प्रकार की मृदा सूखा प्रतिरोधी तथा लवण सहिष्णु फसलों जैसे जौ, कपास, बाजरा, मक्का एवं दालों की खेती को आधार प्रदान करती है।
क्षारीय या लवणीय मृदा
- क्षारीय या लवणीय मृदा को रेह, ऊसर, कल्लर, राकर, थुर तथा चोपन भी कहा जाता है।
- मृदा में नमी, ह्यूमस तथा जीवित सूक्ष्मजीवों का अभाव होता है, जिसके कारण ह्यूमस का निर्माण लगभग अनुपस्थित होता है।
- लवणीय या क्षारीय मृदा अधिकतर अनुपजाऊ होती है।
- मुख्य रूप से शुष्क जलवायु एवं अपर्याप्त जल अपवाह के कारण इस मृदा में अधिक लवण उपस्थित होता है।
- वे शुष्क तथा अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में एवं जलग्रहण तथा दलदली क्षेत्रों में होते हैं। इनकी संरचना रेतीली से लेकर दोमट तक होती है।
क्षारीय मृदा की रासायनिक संरचना
- इस मृदा में नाइट्रोजन तथा कैल्शियम की कमी होती है।
- क्षारीय मृदा में सोडियम क्लोराइड एवं सोडियम सल्फेट उपस्थित होता है, जो मृदा को दलहनी फसलों के लिए उपयुक्त बनाता है।
- अपक्षयित होने पर, अपक्षयित चट्टान के टुकड़े सोडियम, मैग्नीशियम तथा कैल्शियम लवण एवं सल्फ्यूरस अम्ल को उत्पन्न करते हैं।
क्षारीय मृदा का वितरण
- पश्चिमी गुजरात, पूर्वी तट के डेल्टा एवं पश्चिम बंगाल के सुंदरबन क्षेत्रों में लवणीय मृदा अधिक विस्तीर्ण है।
- कच्छ के रण में, दक्षिण-पश्चिम मानसून नमक के कणों को लाता है और वहां परत (क्रस्ट) के रूप में निक्षेपित कर देता है।
- प्राकृतिक कारण: डेल्टाओं में समुद्री जल का प्रवेश लवणीय मृदा की घटना को बढ़ावा देता है। मानव निर्मित कारण: सिंचाई के अत्यधिक उपयोग से सघन कृषि के क्षेत्रों में, विशेष रूप से हरित क्रांति के क्षेत्रों में, उपजाऊ जलोढ़ मृदा लवणीय होती जा रही है।
- शुष्क जलवायविक परिस्थितियों के साथ अत्यधिक सिंचाई केशिका क्रिया को बढ़ावा देती है, जिसके परिणामस्वरूप मृदा की ऊपरी परत पर नमक जमा हो जाता है।
- ऐसे क्षेत्रों में, विशेषकर पंजाब एवं हरियाणा में, किसानों को मृदा में लवणता की समस्या को हल करने के लिए जिप्सम मिलाने की की सलाह दी जाती है।
पीट एवं कच्छ क्षेत्र की मृदा / दलदली मृदा
- वे भारी वर्षा एवं उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहां वनस्पति की अच्छी वृद्धि होती है।
- इस प्रकार, इन क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में मृत कार्बनिक पदार्थ निक्षेपित हो जाते हैं एवं इससे मृदा को एक समृद्ध ह्यूमस तथा जैविक मात्रा प्राप्त होती है।
- इस मृदा में कार्बनिक पदार्थ 40-50 प्रतिशत तक अधिक हो सकती हैं।
- ये मृदा सामान्य रूप से भारी तथा काले रंग की होती है।
पीट मृदा का वितरण
- पीट मृदा बिहार के उत्तरी भाग, उत्तराखंड के दक्षिणी भाग एवं पश्चिम बंगाल, ओडिशा तथा तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में व्यापक रूप से पाई जाती है।
- वे भारत के डेल्टा क्षेत्र में भी पाए जाते हैं।
- केरल के एलेप्पी में, इस मृदा को पश्चजल (बैकवाटर) या केरल के कयाल के साथ कर्री के नाम से जाना जाता है
पीट मृदा की रासायनिक संरचना
- इस मृदा में पोटाश एवं फॉस्फेट की कमी होती है।
- नमक की अधिक मात्रा एवं प्रत्येक दिन उच्च ज्वार से बाढ़ आने से मृदा अनुर्वर हो जाती है।
पीट मृदा में फसलें
- जैसे ही वर्षा समाप्त हो जाती है, पीट मृदा धान की खेती को आधार प्रदान करती करती है।
- बंगाल डेल्टा में, यह जूट एवं चावल के लिए उपयुक्त है एवं मालाबार क्षेत्र में, यह मसालों, रबर तथा चावल के लिए उपयुक्त है।




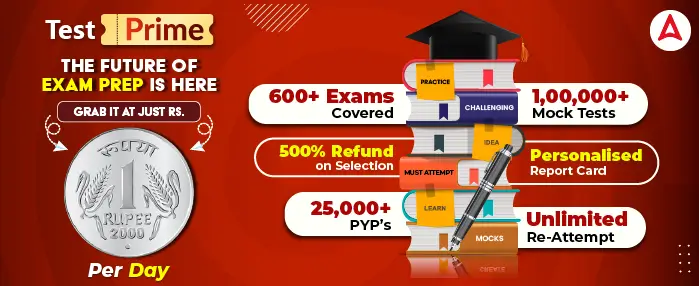
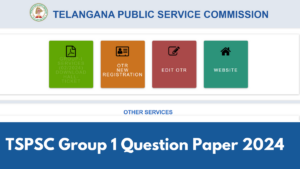 TSPSC Group 1 Question Paper 2024, Downl...
TSPSC Group 1 Question Paper 2024, Downl...
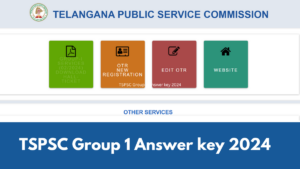 TSPSC Group 1 Answer key 2024 Out, Downl...
TSPSC Group 1 Answer key 2024 Out, Downl...
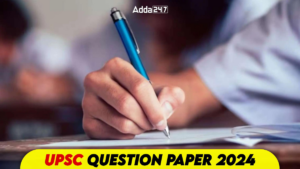 UPSC Prelims 2024 Question Paper, Downlo...
UPSC Prelims 2024 Question Paper, Downlo...