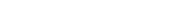Table of Contents
भारत की आर्कटिक नीति- यूपीएससी परीक्षा के लिए प्रासंगिकता
- जीएस पेपर 2: अंतर्राष्ट्रीय भारत के हितों पर विकसित एवं विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीति का प्रभाव।
- जीएस पेपर 3: पर्यावरण- संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण एवं क्षरण।
समाचारों में भारत की आर्कटिक नीति
- हाल ही में, केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ने ‘भारत एवं आर्कटिक: सतत विकास के लिए साझेदारी का निर्माण’ शीर्षक से भारत की आर्कटिक नीति जारी की।
भारत की आर्कटिक नीति
- भारत की आर्कटिक नीति के बारे में: भारत की आर्कटिक नीति जिसका शीर्षक ‘भारत एवं आर्कटिक: सतत विकास के लिए एक साझेदारी का निर्माण’ है।
- भारत की आर्कटिक नीति के क्रियान्वयन हेतु नोडल एजेंसी: राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र (द नेशनल सेंटर फॉर सोलर एंड ओशन रिसर्च/एनसीपीओआर) भारत की आर्कटिक नीति के लिए नोडल संस्थान है।
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र (एनसीपीओआर) भारत के ध्रुवीय अनुसंधान कार्यक्रम के लिए नोडल एजेंसी है।
- भारत की आर्कटिक नीति के स्तंभ: इसके छह स्तंभ हैं जिनका उल्लेख नीचे किया गया है-
- भारत के वैज्ञानिक अनुसंधान एवं सहयोग को सुदृढ़ करना,
- जलवायु तथा पर्यावरण संरक्षण,
- आर्थिक एवं मानव विकास,
- परिवहन तथा कनेक्टिविटी,
- शासन एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, और
- आर्कटिक क्षेत्र में राष्ट्रीय क्षमता निर्माण।
- भारत की आर्कटिक नीति का कार्यान्वयन:
- भारत की आर्कटिक नीति एक कार्य योजना तथा एक प्रभावी शासन एवं समीक्षा तंत्र के माध्यम से क्रियान्वित की जाएगी जिसमें अंतर-मंत्रालयी अधिकार प्राप्त आर्कटिक नीति समूह सम्मिलित है।
- बहु-हितधारक दृष्टिकोण: भारत की आर्कटिक नीति को लागू करने में शिक्षा, अनुसंधान समुदाय, व्यवसाय तथा उद्योग जगत सहित कई हितधारक शामिल होंगे।
भारत की आर्कटिक नीति का महत्व
- भारत आर्कटिक के विभिन्न पहलुओं पर कार्य कर रहे देशों के एक विशिष्ट समूह में सम्मिलित होने हेतु आगे बढ़ा है।
- आर्कटिक परिषद: भारत आर्कटिक परिषद में पर्यवेक्षक का दर्जा रखने वाले तेरह देशों में से एक है।
- आर्कटिक परिषद के बारे में: आर्कटिक परिषद एक उच्च-स्तरीय अंतर-सरकारी मंच है जो आर्कटिक सरकारों एवं आर्कटिक के स्थानिक लोगों के समक्ष उत्पन्न होने वाले मुद्दों को संबोधित करता है।
- पर्यवेक्षक राष्ट्र: तेरह (13) राष्ट्र आर्कटिक परिषद में पर्यवेक्षक हैं- फ्रांस, जर्मनी, इतालवी गणराज्य, जापान, नीदरलैंड, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, पोलैंड, भारत, कोरिया गणराज्य, स्पेन, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड किंगडम।
- आर्कटिक पर भारत का रुख: भारत का कहना है कि समस्त मानवीय गतिविधियां धारणीय, उत्तरदायी, पारदर्शी एवं अंतरराष्ट्रीय कानूनों के प्रति सम्मान पर आधारित होनी चाहिए।
भारत की आर्कटिक नीति के प्रमुख उद्देश्य
भारत की आर्कटिक नीति का उद्देश्य निम्नलिखित कार्य सूची को प्रोत्साहित करना है-
- आर्कटिक क्षेत्र के साथ विज्ञान एवं अन्वेषण, जलवायु तथा पर्यावरण संरक्षण, समुद्री एवं आर्थिक सहयोग में राष्ट्रीय क्षमताओं तथा दक्षताओं को सुदृढ़ करना।
- सरकार एवं शैक्षणिक, अनुसंधान तथा व्यावसायिक संस्थानों के भीतर संस्थागत एवं मानव संसाधन क्षमताओं को सुदृढ़ किया जाएगा।
- आर्कटिक में भारत के हितों की खोज में अंतर-मंत्रालयी समन्वय।
- भारत की जलवायु, आर्थिक एवं ऊर्जा सुरक्षा पर आर्कटिक में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की समझ को बढ़ाना।
- वैश्विक नौवहन मार्गों, ऊर्जा सुरक्षा एवं खनिज संपदा के दोहन से संबंधित भारत के आर्थिक, सैन्य तथा रणनीतिक हितों पर आर्कटिक में बर्फ के पिघलने के प्रभाव पर बेहतर विश्लेषण, पूर्वानुमान एवं समन्वित नीति निर्माण में योगदान देना।
- ध्रुवीय क्षेत्रों तथा हिमालय के मध्य संबंधों का अध्ययन।
- विभिन्न आर्कटिक मंचों के तहत भारत एवं आर्कटिक क्षेत्र के देशों के मध्य सहयोग को और गहन करना, वैज्ञानिक तथा पारंपरिक ज्ञान से विशेषज्ञता प्राप्त करना।
- आर्कटिक परिषद में भारत की सहभागिता में वृद्धि करना एवं आर्कटिक में जटिल शासन संरचनाओं, प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय कानूनों तथा क्षेत्र की भू-राजनीति की समझ में सुधार करना।
निष्कर्ष: भारत की आर्कटिक नीति देश को ऐसे भविष्य के लिए तैयार करने में एक आवश्यक भूमिका निभाएगी जहां मानव जाति की सबसे बड़ी चुनौतियों, जैसे कि जलवायु परिवर्तन, को सामूहिक इच्छा शक्ति एवं प्रयास के माध्यम से हल किया जा सकता है।




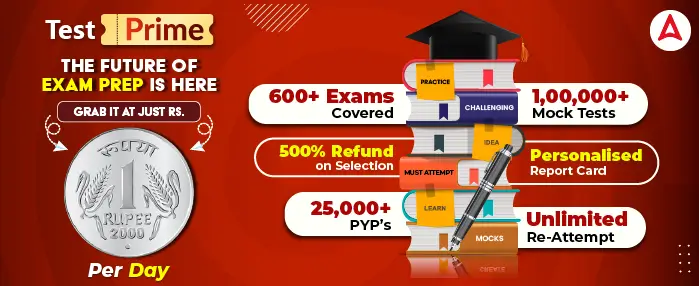
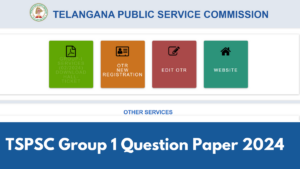 TSPSC Group 1 Question Paper 2024, Downl...
TSPSC Group 1 Question Paper 2024, Downl...
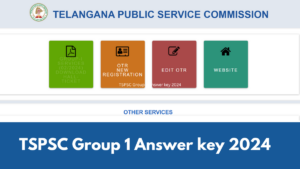 TSPSC Group 1 Answer key 2024 Out, Downl...
TSPSC Group 1 Answer key 2024 Out, Downl...
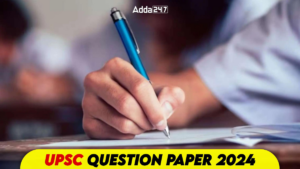 UPSC Prelims 2024 Question Paper, Downlo...
UPSC Prelims 2024 Question Paper, Downlo...