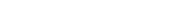Table of Contents
भारत में विभिन्न प्रकार की कृषि
आज भारत में विश्व का दूसरा सर्वाधिक फसल उत्पादन होता है। भारत में विभिन्न प्रकार की कृषि प्रणालियों का अनुसरण उन स्थानों के अनुसार किया जाता है जहां वे सर्वाधिक उपयुक्त हैं। भारत में कृषि क्षेत्र में प्रमुख योगदान देने वाली कृषि प्रणालियाँ निर्वाह कृषि, जैविक कृषि एवं वाणिज्यिक कृषि हैं। भारत की भौगोलिक स्थिति के कारण, इसके कुछ हिस्से भिन्न-भिन्न जलवायु का अनुभव करते हैं, इस प्रकार प्रत्येक क्षेत्र की कृषि उत्पादकता को भिन्न रूप से प्रभावित करते हैं।
भारत में कृषि पद्धतियों को प्रभावित करने वाले कारक
- भूमि की प्रकृति,
- जलवायविक विशेषताएं, एवं
- उपलब्ध सिंचाई सुविधाएं।
यूपीएससी एवं राज्य लोक सेवा आयोगों की परीक्षाओं हेतु नि शुल्क अध्ययन सामग्री प्राप्त करें
भारत में विभिन्न प्रकार की कृषि
स्थानांतरण कृषि
- इस प्रकार की कृषि में वन भूमि के एक टुकड़े को वृक्षों को काटकर एवं टहनियों तथा शाखाओं को जलाकर साफ किया जाता है।
- भूमि को साफ करने के बाद, दो से तीन वर्षों तक फसलें उगाई जाती हैं एवं फिर भूमि की उर्वरता कम होने पर भूमि का परित्याग कर दिया जाता है।
- किसान फिर नए क्षेत्रों में चले जाते हैं और यही प्रक्रिया दोहराई जाती है।
- यह भारत के अधिकांश भागों में विशेष रूप से उत्तर पूर्वी क्षेत्र में प्रचलित है।
निर्वाह कृषि
- निर्वाह कृषि में, एक कृषक एवं उसका परिवार मात्र स्वयं के लिए अथवा स्थानीय बाजार के लिए फसलों का उत्पादन करता है।
- इस प्रकार की कृषि/खेती छोटी एवं बिखरी हुई भूमि जोत तथा साधारण औजारों के उपयोग से अभिलक्षित होती है।
- चूंकि किसान निर्धन हैं, वे अपने खेतों में उर्वरकों तथा उच्च उपज देने वाले बीजों का उपयोग नहीं कर सकते हैं जिससे उनकी उत्पादकता बढ़ सके।
गहन कृषि
- गहन कृषि का लक्ष्य सीमित खेतों में प्रदत परिस्थितियों में सभी संभव प्रयासों के साथ अधिकतम संभव उत्पादन करना है।
- इस प्रकार की कृषि में किसान वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाने में सक्षम होते हैं एवं प्रति हेक्टेयर भूमि पर भारी पूंजी तथा मानव श्रम नियोजित किया जाता है।
- यह हमारे देश के सघन आबादी वाले क्षेत्रों के अधिकांश भागों में प्रचलित है।
विस्तीर्ण कृषि
- विस्तीर्ण कृषि बड़े खेतों पर की जाने वाली खेती की आधुनिक प्रणाली है जिसे मशीनों के व्यापक उपयोग के कारण यांत्रिक कृषि के रूप में भी जाना जाता है।
- विस्तृत खेत में वर्ष में मात्र एक फसल पैदा होती है एवं प्रति हेक्टेयर भूमि की तुलना में श्रम तथा पूंजी का नियोजन सघन कृषि से कम है।
रोपण कृषि
- रोपण कृषि में, झाड़ी या वृक्षों की खेती विशाल क्षेत्रों में की जाती है।
- इस प्रकार की खेती पूंजी केंद्रित होती है एवं इसके लिए उत्तम प्रबंधकीय क्षमता, तकनीकी ज्ञान, उन्नत मशीनरी, उर्वरक एवं सिंचाई तथा परिवहन सुविधाओं की आवश्यकता होती है।
- इसे अन्य खेती के प्रकारों से विभेदित किया जा सकता है क्योंकि रबर, चाय, नारियल, कॉफी, कोको, मसाले एवं फलों इत्यादि की फसल एक विशेष या एकल बोई गई फसल को बोया जाता है एवं उपज आम तौर पर कई वर्षों तक निरंतर प्राप्त की जाती है।
- रोपण कृषि एक निर्यातोन्मुखी कृषि है जहाँ फसल की विपणन क्षमता पर अधिक ध्यान दिया जाता है।
- रोपण कृषि में उत्पादित की जाने वाली अधिकांश फसलों का जीवन चक्र दो वर्ष से अधिक का होता है।
- यह केरल, कर्नाटक, असम एवं महाराष्ट्र में प्रचलित है।
वाणिज्यिक कृषि
- वाणिज्यिक कृषि का प्रचलन व्यापक पैमाने पर फसलों को दूसरे देशों में निर्यात करने एवं देश के विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने की दृष्टि से उत्पादित करने हेतु किया जाता है।
- इस प्रकार की खेती अधिकांशतः विरल आबादी वाले क्षेत्रों में की जाती है।
- यह मुख्य रूप से गुजरात, पंजाब, हरियाणा एवं महाराष्ट्र में प्रचलित है।
- उदाहरण: गेहूं, कपास, गन्ना, मक्का इत्यादि।
शुष्क भूमि कृषि
- शुष्क कृषि अथवा शुष्क भूमि की खेती को उन क्षेत्रों में बिना सिंचाई के फसल उत्पादित करने की पद्धति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जहां वार्षिक वर्षा 750 मिमी – 500 मिमी या उससे भी कम होती है।
- यह कम वर्षा वाले क्षेत्रों में अथवा अपर्याप्त सिंचाई सुविधा वाले क्षेत्रों में प्रचलित कृषि है।
- इस प्रकार की खेती में एक विशेष प्रकार की फसल का उत्पादन करने से से नमी बनी रहती है।
- चना, ज्वार, बाजरा एवं मटर ऐसी फसलें हैं जिन्हें कम पानी की आवश्यकता होती है।
- देश के शुष्क क्षेत्रों जैसे पश्चिमी, उत्तर-पश्चिमी भारत एवं मध्य भारत में शुष्क भूमि पर खेती की जाती है।
आर्द्रभूमि कृषि
- आर्द्रभूमि कृषि मुख्य रूप से वर्षा पर निर्भर करती है, अतः इसे उच्च वर्षा अथवा अच्छी तरह से सिंचित क्षेत्रों में किया जाता है।
- इस प्रकार की खेती में प्रमुख फसलें चावल, जूट एवं गन्ना हैं।
- इस प्रकार की खेती उत्तर, उत्तर-पूर्वी भारत एवं पश्चिमी घाट की ढलानों पर प्रचलित है।
सीढ़ीदार कृषि
- सीढ़ीदार कृषि में, पहाड़ी एवं पर्वतीय ढलानों को काटकर सीढ़ियों/छतों का निर्माण किया जाता है तथा भूमि का उपयोग उसी प्रकार किया जाता है जैसे स्थायी कृषि में किया जाता है।
- समतल भूमि की कमी के कारण, समतल भूमि का एक छोटा टुकड़ा उपलब्ध करने हेतु सीढ़ियों का निर्माण किया जाता है।
- पहाड़ी ढलानों पर सीढ़ियों के निर्माण के कारण मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए भी यह एक प्रभावी तरीका है।




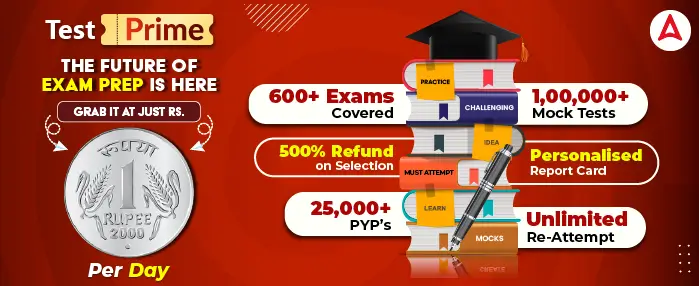
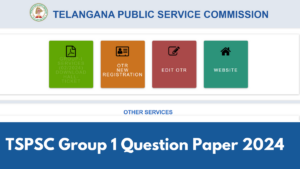 TSPSC Group 1 Question Paper 2024, Downl...
TSPSC Group 1 Question Paper 2024, Downl...
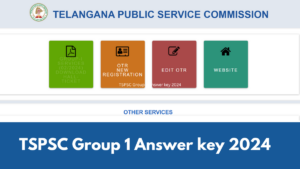 TSPSC Group 1 Answer key 2024 Out, Downl...
TSPSC Group 1 Answer key 2024 Out, Downl...
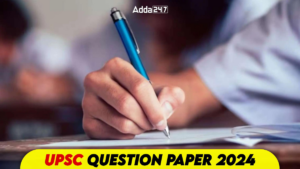 UPSC Prelims 2024 Question Paper, Downlo...
UPSC Prelims 2024 Question Paper, Downlo...