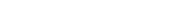Table of Contents
प्रासंगिकता
- जीएस 3: पर्यावरण प्रदूषण एवं अवक्रमण।
प्रसंग
- हाल ही में, एशियन एंड पैसिफिक सेंटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डिजास्टर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट (एपीडीआईएम) ने सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म रिस्क असेसमेंट इन एशिया एंड द पैसिफिक नामक एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें रेत एवं धूल के तूफान के कारण मध्यम एवं उच्च स्तर की खराब वायु गुणवत्ता के वैश्विक जोखिम पर प्रकाश डाला गया है।
- एपीडीआईएम एशिया एवं प्रशांत हेतु संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग (यूएन-ईएससीएपी) की एक क्षेत्रीय संस्था है।
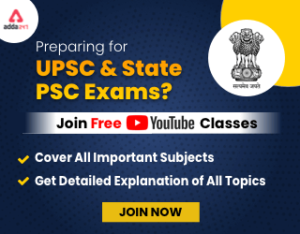
मुख्य बिंदु
- भारत में 500 मिलियन से अधिक व्यक्ति एवं तुर्कमेनिस्तान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान तथा ईरान की 80 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या रेत एवं धूल भरी आंधी के कारण मध्यम एवं उच्च स्तर की खराब वायु गुणवत्ता के प्रति अनावृत है।
- ‘दक्षिण पश्चिम एशिया’ में कराची, लाहौर एवं दिल्ली में वायु की खराब गुणवत्ता में रेत तथा धूल भरी आंधी का महत्वपूर्ण योगदान है।
- 2019 में इन स्थानों पर लगभग 60 मिलियन लोगों ने वर्ष में 170 से अधिक धूल भरे दिनों का अनुभव किया।
आईएमडी एवं भारत में मौसम का पूर्वानुमान
रेत एवं धूल के तूफान क्या हैं?
- रेत एवं धूल भरी आंधी एक सीमापारीय मौसम संबंधी संकट है जो शुष्क एवं अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में सामान्य हैं तथा इस क्षेत्र के विस्तृत हिस्से में फैले हुए हैं।
- प्रमुख घटनाएं धूल का परिवहन अत्यधिक दूरी तक कर सकती हैं ताकि उनका प्रभाव न केवल उन क्षेत्रों में जहां वे उत्पन्न होते हैं, बल्कि स्रोत क्षेत्रों से दूर समुदायों में भी, प्रायः अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के पार होते हैं।
रेत एवं धूल भरी आंधी के मुख्य स्रोत
- एशिया एवं प्रशांत के चार प्रमुख रेत एवं धूल भरी आंधी गलियारे:
- पूर्व एवं पूर्वोत्तर एशिया
- दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिम एशिया,
- मध्य एशिया
- प्रशांत
- यह क्षेत्र खनिज धूल का दूसरा सर्वाधिक वृहद उत्सर्जक है।
हिमालय में जल विद्युत परियोजनाएं
नकारात्मक प्रभाव
- खाद्य सुरक्षा पर
- रेत और धूल भरी आंधी लाखों छोटे कृषकों एवं पशुपालकों की आजीविका एवं खाद्य सुरक्षा को हानि पहुंचाती है, साथ ही उत्पादन को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हुए कृषि की आधारिक संरचना को हानि पहुंचाती है।
- सार्वजनिक स्वास्थ्य पर
- रेत एवं धूल भरी आंधी फेफड़ों के कैंसर तथा तीव्र श्वसन संक्रमण, हृदय एवं श्वसन संबंधी रोगों जैसी पुरानी बीमारियों के लिए एक जोखिम कारक का प्रतिनिधित्व करती है, जिसके परिणामस्वरूप समय पूर्व मृत्यु हो जाती है।
- स्वच्छ जल पर
- पर्यावरण और जल संसाधनों में रेत एवं धूल के स्तर में वृद्धि से जल की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
- दीर्घावधि में, इससे सभी के लिए सुरक्षित एवं वहन योग्य पेयजल उपलब्ध कराने में कठिनाइयां उत्पन्न होंगी।
- आधारिक संरचना पर
- बिजली, पानी, सड़क एवं अन्य महत्वपूर्ण आधारिक संरचना की विफलता रेत एवं धूल भरी आंधी के परिणामस्वरूप घटित हो सकती है जो समुदाय के लिए जीवंत एवं महत्वपूर्ण सेवाओं की उपलब्धता को बाधित कर सकती है।
- हिम (बर्फ) के पिघलने पर
- हिमनदों पर धूल का प्रभाव वैश्विक तापन को प्रेरित करता है, जिससे बर्फ का पिघलना बढ़ जाता है।
सकारात्मक प्रभाव
- धूल भरी आंधी विशेष रूप से निक्षेपण वाले क्षेत्रों के लिए लाभदायक सिद्ध होती है क्योंकि वे पोषक तत्वों की मात्रा में वृद्धि कर सकते हैं जो उस क्षेत्र में वनस्पति की सहायता कर सकते हैं।
- धूल के कण जो लोहे को ले जाते हैं, महासागरों के कुछ हिस्सों को समृद्ध कर सकते हैं, समुद्री खाद्य संजाल के निहितार्थ के साथ, फाइटोप्लांकटन संतुलन को परिवर्तित कर सकते हैं।
- जल निकायों पर निक्षेपित धूल उनकी रासायनिक विशेषताओं को परिवर्तित कर देती है, जिससे सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
जलवायु परिवर्तन एवं धूल भरी आंधी
- जलवायविक परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण, अनेक शुष्क भूमियां शुष्कतर होती जा रही हैं एवं फलस्वरूप वायु अपरदन एवं रेत तथा धूल भरी आंधी के संकट की ओर अधिक प्रवृत्त हैं ।
संस्तुतियां
- क्षेत्र में विभिन्न क्षेत्रों हेतु रेत एवं धूल भरी आंधियों के जोखिम को समझना आपदा जोखिम प्रबंधन को सशक्त करने हेतु आपदा जोखिम शासन को सशक्त करने का आधार है।
- यह प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करने एवं आपदा तत्परता में वृद्धि करने हेतु निवेश के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों तथा भौगोलिक क्षेत्रों के अभिनिर्धारण में भी सहायता करता है।
- रेत एवं धूल भरी आंधियों की सीमापारीय प्रकृति के लिए क्षेत्रीय कार्रवाई एवं अंतर-क्षेत्रीय सहयोग की आवश्यकता होती है।
- स्रोत एवं प्रभाव क्षेत्रों के मध्य आंकड़े साझा करने के साथ-साथ विभिन्न क्षेत्रों में जोखिम साझा करने वाले देशों के मध्य समन्वय हेतु समन्वित कार्रवाई।
- अवसंरचना विकास योजनाओं में आपदाओं के जोखिम पर विचार किया जाना चाहिए क्योंकि यह संपूर्ण क्षेत्र को अनावश्यक आपदा लागतों से बचने में सहायता करता है।
यूएनईपी का कथन: सीसा-युक्त पेट्रोल की पूर्ण रूप से समाप्ति


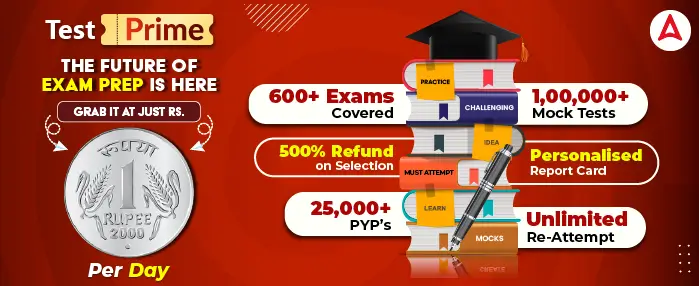
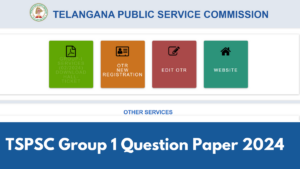 TSPSC Group 1 Question Paper 2024, Downl...
TSPSC Group 1 Question Paper 2024, Downl...
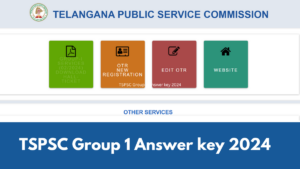 TSPSC Group 1 Answer key 2024 Out, Downl...
TSPSC Group 1 Answer key 2024 Out, Downl...
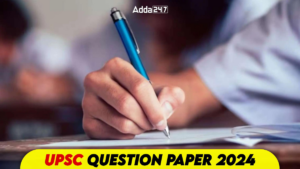 UPSC Prelims 2024 Question Paper, Downlo...
UPSC Prelims 2024 Question Paper, Downlo...