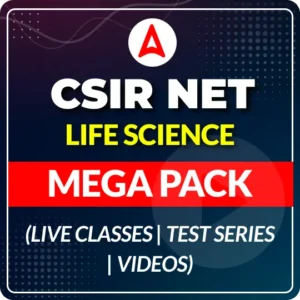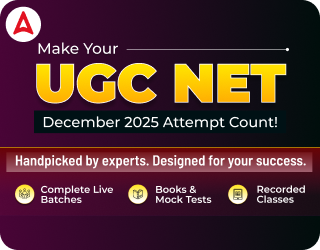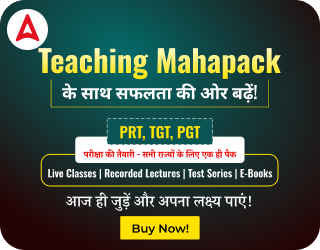Table of Contents
रस – परिभाषा, भेद और उदाहरण is very important topic of Hindi Grammar. Ras in Hindi carries 2-3 objective type questions in CTET, TET exam which are based on रस – परिभाषा, भेद और उदाहरण. Ras in Hindi Vyakaran carries various kind of questions i.e. karun ras kya h ? shok ras kis vakaya me h ? Here we are also going to learn रस – परिभाषा, भेद और उदाहरण in detail.
रस परिभाषा
“विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः।” अर्थात् विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इस प्रकार काव्य पढ़ने, सुनने या अभिनय देखने पर विभाव आदि के संयोग से उत्पन्न होने वाला आनन्द ही ‘रस’ है।
- रस का शाब्दिक अर्थ है – आनन्द।
- भरतमुनि ने अपने ‘नाट्यशास्त्र’ में रस के स्वरूप को स्पष्ट किया था। रस की निष्पत्ति के सम्बन्ध में उन्होंने लिखा है –
- साहित्य को पढ़ने, सुनने या नाटकादि को देखने से जो आनन्द की अनुभूति होती है, उसे ‘रस’ कहते हैं।
रस के चार अंग
रस के मुख्य रुप से चार अंग माने जाते हैं, जो निम्न प्रकार हैं –
- स्थायी भाव – हृदय में मूलरूप से विद्यमान रहने वाले भावों को स्थायी भाव कहते हैं। ये चिरकाल तक रहने वाले तथा रस रूप में सजित या परिणत होते हैं।
स्थायी भावों की संख्या नौ है –
| संख्या | स्थायी भाव | रस |
| 1 | रति | श्रृंगार |
| 2 | हास | हास्य |
| 3 | शोक | करूण |
| 4 | क्रोध | रौद्र |
| 5 | उत्साह | वीर |
| 6 | भय | भयानक |
| 7 | जुगुप्सा(घृणा) | वीभत्स |
| 8 | विस्मय | अद्भुत |
| 9 | निर्वेद (वैराग) | शांत |
2. विभाव – जो व्यक्ति वस्तु या परिस्थितियाँ स्थायी भावों को उद्दीपन या जागृत करती हैं, उन्हें विभाव कहते हैं। विभाव दो प्रकार के होते हैं
(i) आलम्बन विभाव जिन वस्तुओं या विषयों पर आलम्बित होकर भाव उत्पन्न होते हैं, उन्हें आलम्बन विभाव कहते हैं; जैसे – नायक – नायिका।
आलम्बन के दो भेद हैं –
- आश्रय – जिस व्यक्ति के मन में भाव उत्पन्न होते हैं, उसे आश्रय कहते हैं।
- आलम्बन (विषय) – जिस वस्तु या व्यक्ति के लिए आश्रय के मन में भाव उत्पन्न होते हैं, उसे आलम्बन या विषय कहते हैं।
- उद्दीपन विभाव – स्थायी भाव को तीव्र करने वाले कारक उद्दीपक विभाव कहलाते है।
3. अनुभाव – आलम्बन तथा उद्दीपन के द्वारा आश्रय के हृदय में शीरीरकि व मानसित चेष्टाएँ उत्पन्न होती हैं, उन्हें अनुभाव कहते हैं। अनुभाव चार प्रकार के माने गए है – कायिक (शारीरिक चेष्टाये जैसे – इशारे, उच्छवास, कटाक्ष), मानसिक, आहार्य और सात्विका सात्विक अनुभाव की संख्या आठ है, जो निम्न प्रकार है –
- स्तम्भ
- स्वेद
- रोमांच
- स्वर – भंग
- कम्प
- विवर्णता (रंगहीनता)
- अक्षु
- प्रलय (संज्ञाहीनता)
4. संचारी भाव (व्यभिचारी भाव) – आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अल्पकालिक मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। इनके द्वारा स्थायी भाव और तीव्र हो जाता है।
- संचारी भावों की संख्या 33 है – हर्ष, विषाद, त्रास, लज्जा (व्रीड़ा), ग्लानि, चिन्ता, शंका, असूया, अमर्ष, मोह, गर्व, उत्सुकता, उग्रता, चपलता, दीनता, जड़ता, आवेग, निर्वेद, धृति, मति, विबोध, वितर्क, श्रम, आलस्य, निद्रा, स्वप्न, स्मृति, मद, उन्माद, अवहित्था, अपस्मार, व्याधि, मरण।
- आचार्य देव कवि ने ‘छल’ को चौतीसवाँ संचारी भाव माना है।
रस के प्रकार
वस्तुतः रस की संख्या 9 ही है।
- श्रृंगार रस
- करुण रस
- हास्य रस
- वीर रस
- रौद्र रस
- भयानक रस
- बीभत्स रस
- अद्भुत रस
- शान्त रस
- वात्सल्य रस
- भक्ति रस
शृंगार रस
कामभावना अथवा कामदेव के जागृत होने को शृंङ्ग कहते हैं। अतः इस रस का आधार स्त्री – पुरुष का सहज आकर्षण है। जब प्रेमियों में सहज रूप से विद्यमान रति नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से आस्वाद के योग्य (आनंद प्राप्त करने योग्य) हो जाता है, तो उसे शृंगार रस कहते हैं। शृंगार रस में सुखद एवं दुखद दोनों प्रकार की अनुभूतियाँ होती हैं। इस आधार पर इस रस के दो भेद माने गए हैं – संयोग शृंगार एवं वियोग या विप्रलंभ शृंगार।
करुण रस
इष्ट वस्तु – वैभव आदि का नाश, अनिष्ट की प्राप्ति, प्रेम पात्र का चिर वियोग प्रियजन की पीड़ा अथवा मृत्यु की प्राप्ति अर्थ हानि आदि से जहाँ शोक भाव की परिपूष्टि होती है, वहाँ करुण रस होता है। करुण रस जीवन में सहानुभूति की भावना का विस्तार करता है तथा मनुष्य को भोग की अपेक्षा साधना की ओर अग्रसर करता है, अतः महत्त्वपूर्ण माना जाता है।
उदाहरण –
मात को मोह, ना द्रोह’ विमात को सोच न तात’ के गात दहे’को,
प्रान को छोभ न बंधु बिछोभ न राज को लोभ न मोद रहे’ को।
एते पै नेक न मानत ‘श्रीपति’ एते मैं सीय वियोग सहे को।।
तारन – भूमि” मैं राम कह्यो, मोहि सोच विभीषन भूप कहे को।।
हास्य रस
इसका स्थायी भाव हास है। जब नायक – नायिका में कुछ अनौचित्य का आभास मिलता है, तो यह भाव जागृत हो जाता है। साधारण से भिन्न व्यक्ति, वस्तु, आकृति, विचित्र वेशभूषा, असंगत क्रियाओं, विचारों, व्यापारों, व्यवहारों को देखकर जिस विनोद भाव का संचार होता है, उसे हास कहते हैं। नीचे की पंक्तियों में उस रजाई की क्षीणता का वर्णन है –
कारीगर कोऊ करामात कै बनाइ लायो;
लीन्हों दाम थोरो जानि नई सुघरई है।
रायजू ने रामजू रजाई दीन्हीं राजी ढके,
सहर में ठौर – ठौर सोहरत भई है।।
बेनी कवि पाइकै, अघाई रहे घरी वैके,
कहत न बने कछू ऐसी मति ठई है।
सांस लेत उडिगो उपल्ला औ भितल्ला सबै,
दिन वैके बाती हेत रुई रहि गई है।
वीर रस
उत्साह स्थायी भाव जब विभावों, अनुभावों और संचारी भावों से पुष्ट होकर आस्वादन के योग्य होता है, तब उसे वीर रस कहते हैं। उत्साह के चार क्षेत्र पाए गए हैं – युद्ध, धर्म, दया और दान। जब इन क्षेत्रों में उत्साह रस की कोटि तक पहुँचता है, तब उसे वीर रस कहते हैं।
उदाहरण –
मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे।
यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे।
है और की तो बात ही क्या गर्व मैं करता नहीं।
मामा तथा निज तात से भी समर में डरता नहीं।
– मैथिलीशरण गुप्त
रौद्र रस
रस क्रोध के कारण उत्पन्न इन्द्रियों की प्रबलता को रौद्र कहते हैं। किसी विरोधी, अपकारी, धृष्ट आदि के कार्य या चेष्टाएँ, असाधारण अपराध, अपमान या अहंकार, पूज्य जन की निंदा या अवहेलना आदि से उसके प्रतिशोध में जिस क्रोध का संचार होता है, वही रौद्र रस के रूप में व्यक्त होता है।
उदाहरण –
अब जनि देइ दोसु मोहि लोगू। कटुवादी बालक वध जोगू॥
बाल विलोकि बहुत मैं बाँचा। अब येहु मरनहार भा साँचा॥
खर कुठार मैं अकरुन कोही। आगे अपराधी गुरुद्रोही॥
उत्तर देत छोडौं बिनु मारे। केवल कौशिक सील तुम्हारे ॥
न त येहि काटि कुठार कठोरे। गुरहि उरिन होतेउँ भ्रम थोरे ॥
भयानक रस
डरावने दृश्य देखकर मन में भय उत्पन्न होता है। जब भय नामक स्थायीभाव का मेल विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से होता है, तब भयानक रस उत्पन्न होता है।
उदाहरण –
प्रलय का एक भयानक चित्र देखिए –
पंचभूत का वैभव मिश्रण झंझाओं का सकल निपातु,
उल्का लेकर सकल शक्तियाँ, खोज रही थीं खोया प्रात।
धंसती धरा धधकती ज्वाला, ज्वालामुखियों के नि:श्वास;
और संकुचित क्रमशः उसके अवयव का होता था ह्रास।
वीभत्स रस
वीभत्स का स्थायी भाव जुगुप्सा है। अत्यंत गंदे और घृणित दृश्य वीभत्स रस की उत्पत्ति करते हैं। गंदी और घृणित वस्तुओं के वर्णन से जब घृणा भाव पुष्ट होता है तब यह रस उत्पन्न होता है।
उदाहरण –
हाथ में घाव थे चार
थी उनमें मवाद भरमार
मक्खी उन पर भिनक रही थी,
कुछ पाने को टूट पड़ी थी
उसी हाथ से कौर उठाता
घृणा से मेरा मन भर जाता।
अद्भुत रस
इसका स्थायी भाव विस्मय है। किसी असाधारण व्यक्ति, वस्तु या घटना को देखकर जो आश्चर्य का भाव जागृत होता है, वही अद्भुत रस में परिणत होता है।
उदाहरण –
गोपी ग्वाल माली’ जरे आपुस में कहैं आली।
कोऊ जसुदा के अवतर्यो इन्द्रजाली है।
कहै पद्माकर करै को यौं उताली जापै,
रहन न पाबै कहूँ एकौ फन’ खाली है।
देखै देवताली भई विधि’ कै खुसाली कूदि,
किलकति काली” हेरि हंसत कपाली हैं।
जनम को चाली’ परी अद्भुत है ख्याली’ आजु,
काली’ की फनाली” पै नाचत बनमाली है।।
शांत रस
शम (शांत हो जाना) या निर्वेद (वेदना रहित) नामक स्थायी भाव इसका आधार है। ईश्वरीय प्राप्ति से प्राप्त होने वाले परम आनंद की स्थिति में सारे मनोविकार शांत हो जाते हैं और एक अनुपम शांति का अनुभव होने लगता है। यह शांति सांसारिक विषय – वासनाओं से प्राप्त सुख से सर्वथा भिन्न होती है। इसी आधार पर नाट्यशास्त्र में नाटक में शांत रस की स्थिति स्वीकार नहीं की गई है।
उदाहरण –
सुत बनितादि जानि स्वारथ रत न करु नेह सबही ते।
अंतहिं तोहि तजेंगे पामर! तूं न तजै अबही ते।।
अब नाथहिं अनुराग जागु जड़, त्यागु दुरासा जीते।
बुझे न काम, अगिनी ‘तुलसी’ कहुँ विषय भोग बहु घी ते।। – तुलसी (विनयपत्रिका)
वात्सल्य रस
इसे रस का अलग भेद मानने के संबंध में मतभेद है किंतु तुलसी, सूर आदि ने वात्सल्य रस की अनेक अनुपम कृतियाँ हमें भेंट की हैं। बच्चों की मोहक बातों और गतिविधियों में स्वाभाविक आकर्षण होता है। इस आकर्षण में निहित स्नेह भाव की व्यंजना में ही वात्सल्य रस की निष्पत्ति होती है। अतः वात्सल्य भाव ही इसका स्थायी है,
उदाहरण –
कबहूँ ससि माँगत आरि करें कबहूँ प्रतिबिंब निहारि डरैं।
कबहूँ करताल बजाइ के नाचत मातु सबै मन मोद भरें।।
कबहूँ रिसिआई करें हठि के पनि लेत सोई जेहि लागि अरें।
अवधेस के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में विहरैं। – तुलसी (कवितावली)
भक्ति रस
भक्ति रस में भी प्रेम का परिपाक होता है, किंतु यहाँ रति भाव इष्टदेव के प्रति होता है। जब विषयादि के संयोग से आराध्य विषयक प्रेम का संचार होता है, तब वहाँ भक्ति रस की व्यंजना होती है। कुछ विद्वान इसे शृंगार रस के अंतर्गत ही स्थान देते हैं, किंतु भक्ति भावना का आस्वाद और उत्कटता किसी भी प्रधान रस से कम नहीं है। यह सांसारिक शृंगार से कहीं अधिक उदात्त भाव है। भक्त कवियों की रचनाएँ इसका प्रमाण हैं।
उदाहरण –
मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई।
जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई।।
साधुन संग बैठि – बैठि, लोक लाज खोई।
अब तो बात फैल गई, जानत सब कोई।।
असुअन जल सींचि – सींचि प्रेम बेलि बोई।।
मारां को लगन लागी होनी होइ सो होई।
Download रस Study Notes PDF
The direct link to Download रस Study Notes PDF has been provided below. Click on the below link to check the Hindi Grammar Study Notes PDF.

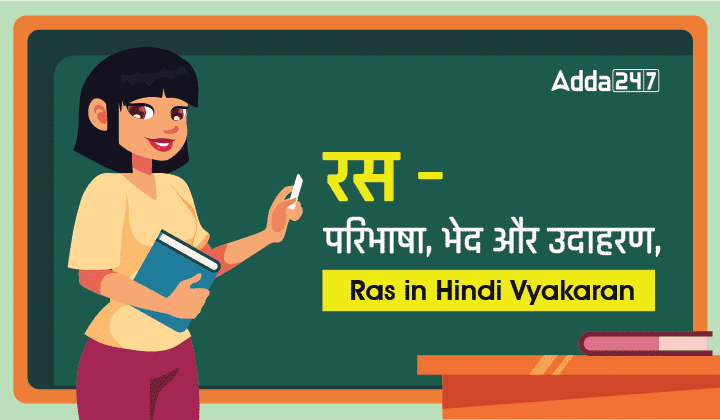
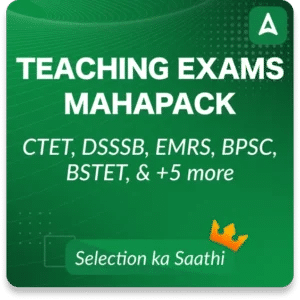
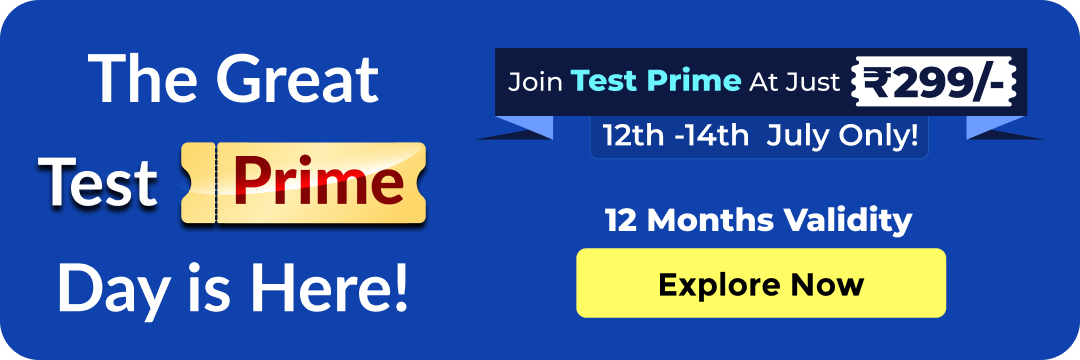
 Phases of Teaching - Stages of Teaching ...
Phases of Teaching - Stages of Teaching ...
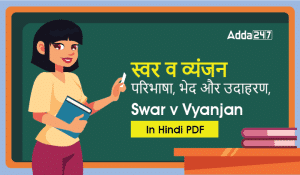 स्वर व व्यंजन - �...
स्वर व व्यंजन - �...
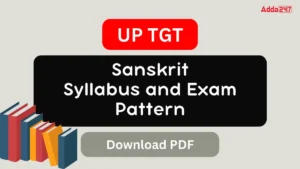 UP TGT Sanskrit Syllabus and Exam Patter...
UP TGT Sanskrit Syllabus and Exam Patter...