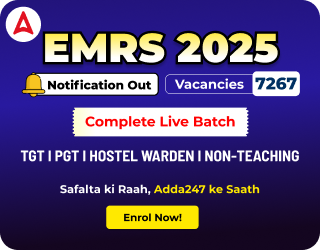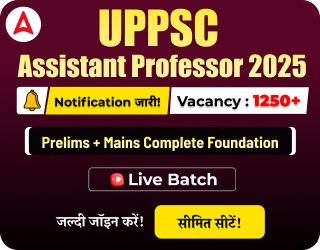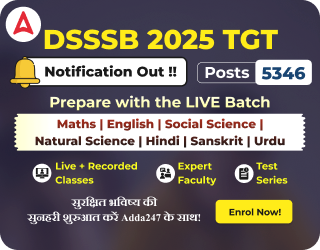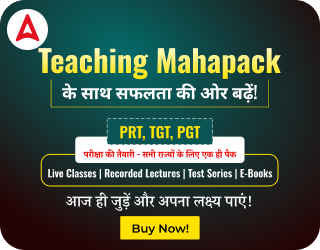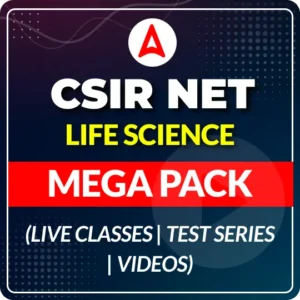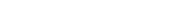Table of Contents
अनुप्रास अलंकार परिभाषा
जिसको वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति से बनाया जाता है, उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। आवृत्ति का अर्थ है कि कोई वर्ण या ध्वनि वाक्य में बार-बार पुनरावृत्त होती है। इस अलंकार का नाम ‘अनुप्रास’ दो शब्दों, ‘अनु’ और ‘प्रास’, के संयोजन से बना है। ‘अनु’ शब्द का अर्थ होता है ‘बार-बार’ और ‘प्रास’ शब्द का अर्थ होता है ‘वर्ण’। जहाँ स्वरों की समानता के बिना भी वर्णों की बार-बार आवृत्ति होती है, वहाँ हम अनुप्रास अलंकार का प्रयोग करते हैं।
अनुप्रास अलंकार के उदाहरण:
- “जन रंजन मंजन दनुज मनुज रूप सुर भूप”। इसमें ‘म’ वर्ण की आवृत्ति द्वारा संगीतमयता आती है।
- “मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए”। इसमें पहले पद में ‘म’ वर्ण की आवृत्ति और दूसरे में ‘स’ वर्ण की आवृत्ति से संगीतमयता प्रकट होती है।
अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं
अनुप्रास अलंकार का उपयोग अक्सर कविता, काव्य, उपन्यास, और अन्य लेखन के रूप में होता है ताकि पाठक विशेष ध्वनियों और शब्दों के संगठन का आनंद ले सकें। इससे न केवल पाठक की ध्यान आकर्षित होती है, बल्कि यह लेखक की कला और व्यक्तिगत शैली को प्रकट करने में भी मदद करता है।
Anupras Alankar उदाहरण
- कालिंदी कूल कदंब की डारिन
- राम नाम-अवलंब बिनु परमार्थ की आस , बरसत बारिद बूँद गहि चाहत चढ़न अकास।
- कल कानन कुंडल मोर पखा उर पे बनमाल विराजती है
- विमल वाणी ने वीणा ली ,कमल कोमल क्र में सप्रीत।
- रघुपति राघव राजा राम
- कालिका सी किलकि कलेऊ देती काल को
- कूकै लगी कोयल कदंबन पर बैठी फेरि।
- तरनि तनूजा तट तमाल तरुवर बहु छाए.
- प्रतिभट कटक कटीले केते काटि काटि
- बरसत बारिद बून्द गहि
- चमक गई चपला चम चम
- कुकि कुकि कलित कुंजन करत कलोल)
- रावनु रथी विरथ रघुवीरा
- खेदी -खेदी खाती दीह दारुन दलन की
- चरर मरर खुल गए अरर रवस्फुटों से।
- मुदित महिपति मंदिर आए। सेवक सचिव सुमंत बुलाए
- गुरु पद रज मृदु मंजुल
- काकी कंकु दे
- बंदौ गुरु पद पदुम परगा। सुरुचि सुबास सरस अनुरागा
- चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में
अनुप्रास अलंकार के प्रकार
अनुप्रास के 5प्रकार है-
- छेकानुप्रास अलंकार
- वृत्यनुप्रास अलंकार
- लाटानुप्रास अलंकार
- अन्त्यानुप्रास अलंकार
- श्रुत्यानुप्रास अलंकार
छेकानुप्रास अलंकार
जब किसी वाक्यांश में अनुक्रमिक रूप से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार होती है, तो उसे ‘छेकानुप्रास’ अलंकार कहते हैं। इस अलंकार में व्यंजनों का उसी अनुक्रम में प्रयोग होता है।
उदाहरण : रीझि रीझि रहसि रहसि हँसि हँसि उठै साँसैं भरि आँसू भरि कहत दई दई। यहाँ ‘रीझि रीझ’, ‘रहसि-रहसि’, ‘हँसि-हँसि’ और ‘दई-दई’ में छेकानुप्रास है, क्योंकि व्यंजनों की आवृत्ति उसी क्रम और स्वरूप में होती है।
वृत्यनुप्रास अलंकार
जब किसी वाक्यांश में एक ही व्यंजन एक या अनेक बार आवृत्ति होती है, तो उसे ‘वृत्यनुप्रास’ अलंकार कहते हैं। इसमें व्यंजनवर्णों का आवृत्ति केवल स्वरूपतः होती है, क्रमतः नहीं।
उदाहरण:
- सपने सुनहले मन भाये।
- सेस महेस गनेस दिनेस सुरेसहु जाहि निरन्तर गावैं।
इन उदाहरणों में ‘स’ वर्ण की आवृत्ति एक बार और अनेक बार होती है, परंतु व्यंजनों का स्वरूपतः आवृत्ति केवल एक ही बार होती है।
लाटानुप्रास अलंकार
जब किसी शब्द या वाक्यांश की आवृत्ति उसी अर्थ में होती है, परंतु तात्पर्य या अन्वय में भिन्नता होती है, तो वहाँ ‘लाटानुप्रास’ अलंकार होता है। इस अलंकार में शब्दों की आवृत्ति तो समान होती है, परंतु उनका अर्थ या भाव भिन्न होता है।
उदाहरण:
- तेगबहादुर, हाँ, वे ही थे गुरु-पदवी के पात्र समर्थ,
- तेगबहादुर, हाँ, वे ही थे गुरु-पदवी थी जिनके अर्थ।
इन उदाहरणों में ‘तेगबहादुर’ के आवृत्ति तो एक समान है, परंतु दोनों वाक्यों में उसका तात्पर्य या अन्वय भिन्न है। पहले वाक्य में उसका तात्पर्य ‘गुरु-पदवी के पात्र समर्थ’ होता है, जबकि दूसरे वाक्य में उसका तात्पर्य ‘गुरु-पदवी थी जिनके अर्थ’ से होता है। इस प्रकार, इस अलंकार से शब्दों और अर्थ के मध्य विभिन्नता प्रकट होती है।
अन्त्यानुप्रास अलंकार
जब किसी वाक्य या शब्द में अंत में तुक मिलती है, तो वहाँ ‘अन्त्यानुप्रास अलंकार’ होता है।
अन्त्यानुप्रास अलंकार के उदाहरण निम्न प्रकार है:
- लगा दी किसने आकर आग।
- कहाँ था तू संशय के नाग?
श्रुत्यानुप्रास अलंकार
जब कानों को मधुर लगने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है, तो वहाँ ‘श्रुत्यानुप्रास अलंकार’ होता है।
श्रुत्यानुप्रास अलंकार के उदाहरण निम्न प्रकार है:
- दिनान्त था, थे दीननाथ डुबते,
- सधेनु आते गृह ग्वाल बाल थे।

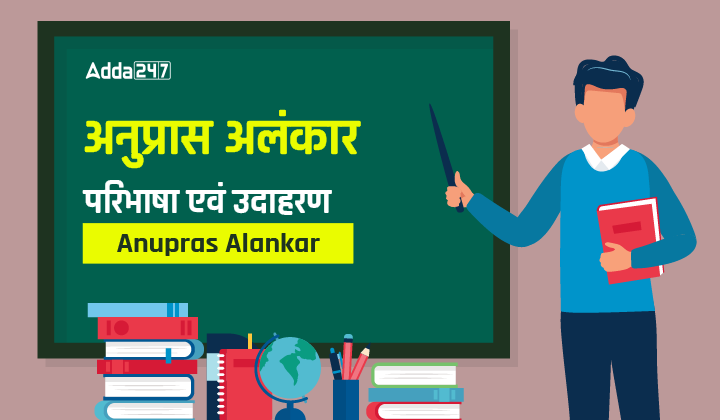
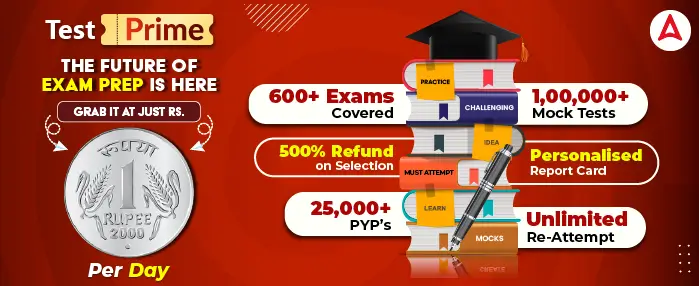
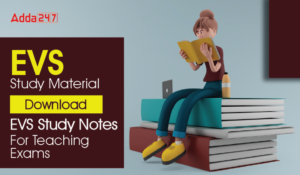 EVS Notes For CTET and TETs Exam, Downlo...
EVS Notes For CTET and TETs Exam, Downlo...
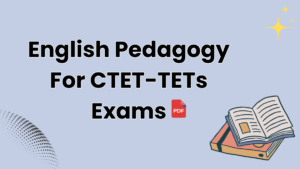 English Pedagogy Study Notes & Quest...
English Pedagogy Study Notes & Quest...
 UGC NET Study Notes for Paper 1, Downloa...
UGC NET Study Notes for Paper 1, Downloa...