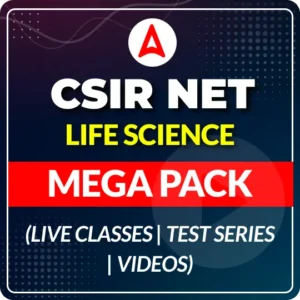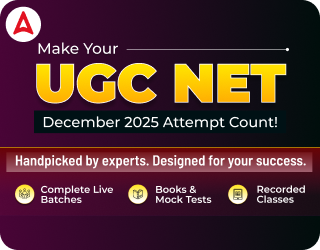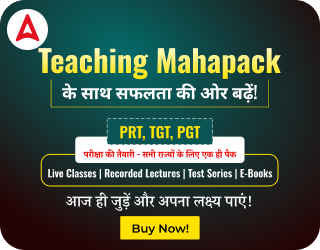Table of Contents
कारक, Karak को हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण विषय माना जाता है। यह विषय शिक्षण परीक्षाओं में 2-3 अंकों का होता है। कारक के बारे में विस्तृत जानकारी के साथ परिभाषा, भेद और उदाहरण दिए जाते हैं। कारक (Karak) हिंदी में सरल और अंक ग्रहण के लिए सुलभ विषय है। भर्ती परीक्षाओं में कारक विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के साथ पूछा जाता है, जैसे कारक के उदाहरण क्या है? कारक से क्या अभिप्राय है? इसके उदाहरण के साथ प्रत्येक उदाहरण को इस जगह से सीख सकते हैं।
कारक से क्या अभिप्राय है?
कारक शब्द का शाब्दिक अर्थ है – करने वाला अर्थात क्रिया को पूरी तरह करने में किसी न किसी भूमिका को निभाने वाला। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रुप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से पता चले, उसे कारक कहते है।
कारक का अर्थ है किसी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया या किसी अन्य शब्द के साथ संबंध। यह संबंध विभिन्न प्रकार का हो सकता है, जैसे कि कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, और सम्बोधन।
विभक्ति या परसर्ग
कारकों का रुप प्रकट करने के लिये उनके साथ जो शब्द चिन्ह लगते है, उन्हें विभक्ति कहते है। इन कारक चिन्हों या विभक्तियों को परसर्ग भी कहते है। जैसे – ने, में, को, से।
Karak Kise Kahate Hain
कारक (हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण भाग है जो किसी क्रिया के संदर्भ को स्पष्ट करने के लिए प्रयुक्त होता है। कारक का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि क्रिया किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ कैसे हो रही है, या क्रिया को कैसे किया जा रहा है। कारक की मदद से क्रिया के कर्ता, विधि, उपकरण, प्राप्य, समय, स्थान, कारण, आदि के संदर्भ को स्पष्ट किया जा सकता है।
कारक विभक्ति क्या है?
हिंदी व्याकरण में कारक विभक्ति एक महत्वपूर्ण विषय है, जो वाक्य निर्माण और शब्दों के संबंध को समझने में मदद करता है। “कारक” का अर्थ है ‘क्रिया’ के साथ किसी संज्ञा या सर्वनाम का संबंध और “विभक्ति” का मतलब है ‘रूप परिवर्तन’। इसलिए, कारक विभक्ति वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा संज्ञा या सर्वनाम का रूप बदलता है ताकि वह वाक्य में अपने सही अर्थ को प्रकट कर सके।
कारक और विभक्ति चिन्ह
- कारक (Karak) : किसी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ जो संबंध होता है, उसे कारक कहते हैं। कारक यह बताते हैं कि वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से क्या संबंध है। हिंदी व्याकरण में कारकों की संख्या आठ होती है। उदाहरण: राम ने फल खाया। (यहाँ “राम” कर्ता कारक है।), सीता ने राम को देखा। (यहाँ “राम” कर्म कारक है।)
- विभक्ति चिन्ह (Vibhakti Chinha): कारकों के साथ जो चिन्ह (जैसे: ने, को, से, का, में, पर आदि) लगाए जाते हैं, उन्हें विभक्ति चिन्ह कहते हैं। ये चिन्ह संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगकर उनका क्रिया के साथ संबंध स्थापित करते हैं। उदाहरण: राम ने खाना खाया। (यहाँ “ने” विभक्ति चिन्ह है।), वह पेड़ से गिर गया। (यहाँ “से” विभक्ति चिन्ह है।)
हिंदी में कारकों को विभक्ति चिन्हों द्वारा प्रकट किया जाता है, जो संज्ञा या सर्वनाम के अंत में जोड़े जाते हैं। उदाहरण के लिए:
| कारक (Karak) | कारक के भेद | विभक्ति चिन्ह (Vibhakti Chinha) | उदाहरण |
|---|---|---|---|
| कर्ता (Karta) | कर्ता कारक | ने (Ne) | राम ने खाना खाया। |
| कर्म (Karma) | कर्म कारक | को (Ko) | सीता ने राम को देखा। |
| करण (Karan) | करण कारक | से (Se), के द्वारा (Ke Dwara) | वह कलम से लिखता है। |
| संप्रदान (Sampradan) | संप्रदान कारक | को (Ko), के लिए (Ke Liye) | मैंने बच्चे को किताब दी। |
| अपादान (Apadan) | अपादान कारक | से (Se) | वह पेड़ से गिर गया। |
| संबंध (Sambandh) | संबंध कारक | का, की, के (Ka, Ki, Ke) | यह राम की किताब है। |
| अधिकरण (Adhikaran) | अधिकरण कारक | में, पर (Mein, Par) | किताब मेज पर रखी है। |
| संबोधन (Sambodhan) | संबोधन कारक | हे, अरे, ओ (He, Are, O) | हे राम! कैसे हो? |
कारक के भेद Karak in Hindi
कारक के कुल भेद आठ होते हैं, जिनके नाम हैं, कर्ता, कर्म, करण, सम्प्रदान, आपादान, सम्बन्ध,अधिकरण और संबोधन कारक हैं।
| विभक्ति | कारक | क्रिया चिन्ह |
| प्रथमा | कर्ता | ने |
| द्वितीया | कर्म | को |
| तृतीया | करण | से, के द्वारा |
| चतुर्थी | सम्प्रदान | के लिए , को |
| पंचमी | अपादान | से (अलग होने के अर्थ में) |
| षष्ठी | सम्बन्ध | का, के, की |
| सप्तमी | अधिकरण | में, पर |
| सम्बोधन | सम्बोधन | हे! ओर! |
1. कर्ता कारक – Karta Karak
क्रिया के करने वाले को कर्ता कारक कहतें है। यह पद प्रायः संज्ञा या सर्वनाम होता है। इसका सम्बन्ध क्रिया से होता है। जैसे – राम ने पत्र लिखा । यहाँ कर्ता राम है। जैसे – बालक लिखता है (वर्तमान काल), रमेश घर जायगा। (भविष्य काल)
कर्ता कारक का प्रयोग दो प्रकार से होता है –
- परसर्ग सहित – जैसे – राम ने पुस्तक पढ़ी। यहाँ कर्ता के साथ ‘ने’ परसर्ग है । भूतकाल की सकर्मक क्रिया होने पर कर्ता के साथ ‘ने’ परसर्ग लगाया जाता है।
- परसर्ग रहित – (क) भूतकाल की अकर्मक क्रिया के साथ परसर्ग ‘ने’ नही लगता| जैसे – राम गया। मोहन गिरा। वर्तमान और भविष्यत काल में परसर्ग का प्रयोग नहीं होता।
2. कर्म कारक -Karm Karak
जिस वस्तु पर क्रिया का फल पड़ता है, संज्ञा के उस रुप को कर्म कारक कहते है। इसका विभक्ति चिन्ह ‘को’ है।
कर्म कारक के उदाहरण
- राम ने रावण को मारा । यहाँ मारने की क्रिया का फल रावण पर पड़ा है।
- उसने पत्र लिखा । यहाँ लिखना क्रिया का फल ‘पत्र’ पर है, अतः पत्र कर्म है।
3. करण कारक – Karan Karak
संज्ञा के जिस रुप से क्रिया के साधन का बोध हो, उसे करण कारक कहते है। इसका विभक्ति चिन्ह है – से (द्वारा)
करण कारक के उदाहरण
- राम ने रावण को बाण से मारा। यहाँ राम बाण से या बाण द्वारा रावण को मारने का काम करता है। यहाँ ‘बाण से’ करण कारक है।
4. सम्प्रदान कारक – Sampradan Karak
सम्प्रदान का अर्थ है देना । जिसे कुछ दिया जाए या जिसके लिए कुछ किया जाए उसका बोध कराने वाले संज्ञा के रुप को सम्प्रदान कारक कहते है। इसका विभक्ति चिन्ह ‘के लिए’ या ‘को है।
सम्प्रदान कारक के उदाहरण
- मोहन ब्राह्मण को दान देता है या मोहन ब्राह्मण के लिए दान देता है। यहाँ ब्राह्मण को या ब्राह्मण के लिए सम्प्रदान कारक है।
5. अपादान कारक – Apadan karak
संज्ञा के जिस रुप से अलगाव का बोध हो उसे अपादान कारक कहते है। इसका विभक्ति चिन्ह से’ है।
अपादान कारक के उदाहरण
- वृक्ष से पत्ते गिरते हैं ।
- मदन घोड़े से गिर पड़ा। यहाँ वृक्ष से और घोड़े से अपादान कारक है । अलग होने के अतिरिक्त निकलने, सीखने, उरने, लजाने, अथवा तुलना करने के भाव में भी इसका प्रयोग होता है।
-
- निकलने के अर्थ में – गंगा हिमालय से निकलती है।
- उरने के अर्थ में – चोर पुलिस से उरता है।
- सीखने के अर्थ में – विद्यार्थी अध्यापक से सीखते है।
- लजाने के अर्थ में – वह ससुर से लजाती है।
- तुलना के अर्थ में – राकेश रुपेश से चतुर है।
- दूरी के अर्थ में – पृथ्वी सूर्य से दूर है।
6. सम्बन्ध कारक -Sambhndh Karak
संज्ञा या सर्वनाम के जिस रुप से उसका सम्बन्ध वाक्य की दूसरी संज्ञा से प्रकट हो, उसे सम्बन्ध कारक कहते हैं। इसके परसर्ग हैं – का, के, की, ना, ने, नो, रा,रे,री आदि ।
सम्बन्ध कारक के उदाहरण
- राजा दशरथ का बड़ा बेटा राम था।
- राजा दशरथ के चार बेटे थे।
- राजा दशरथ की तीन रानियाँ थी।
7. अधिकरण कारक – Adhikaran Karak
अधिकरण का अर्थ है आधार या आश्रय । संज्ञा या सर्वनाम के जिस रुप से क्रिया के आधार (स्थान, समय, अवसर आदि) का बोध हो, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इस कारक के विभक्ति चिन्ह हैं – में, पे, पर ।
अधिकरण कारक के उदाहरण
- उस कमरे में चार चोर थे
- मेज पर पुस्तक रखी थी।
8. सम्बोधन कारक – Sanbodhan karak
शब्द के जिस रुप से किसी को सम्बोधित किया जाए या पुकारा जाए, उसे सम्बोधन कारक कहते हैं। इसमें ‘हे’, ‘अरे’ का प्रयोग किया जाता है।
सम्बोधन कारक के उदाहरण
- हे प्रभों, क्षमा करो। अरे बच्चो, शान्त हो जाओ।
विशेष :- कभी – कभी नाम पर जोर देकर सम्बोधन का काम चला लिया जाता है। वहाँ कारक चिन्हों की आवश्यकता नही होती। जैसे – अरे । आप आ गए। अजी। इधर तो आओ।
Karak Study Notes PDF
The direct link to download कारक Study Notes has been provided below. Candidate can download PDF through the below link to know more about the कारक – परिभाषा, भेद और उदहारण

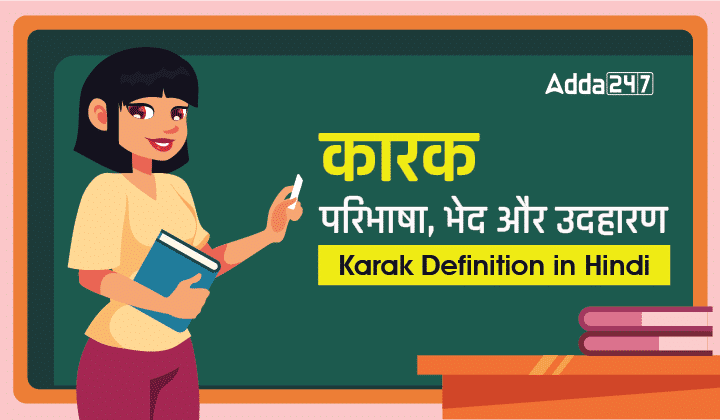

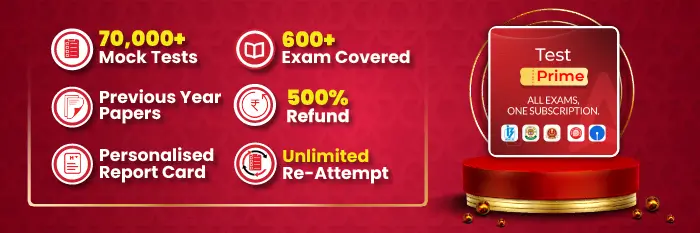
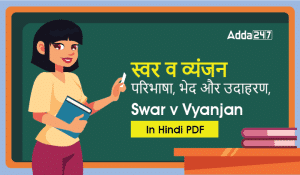 स्वर व व्यंजन - �...
स्वर व व्यंजन - �...
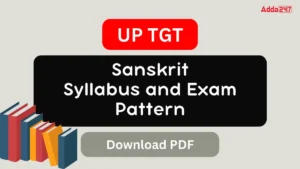 UP TGT Sanskrit Syllabus and Exam Patter...
UP TGT Sanskrit Syllabus and Exam Patter...
 UGC NET Study Notes for Paper 1, Downloa...
UGC NET Study Notes for Paper 1, Downloa...