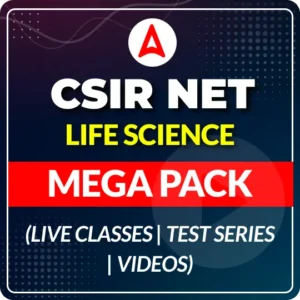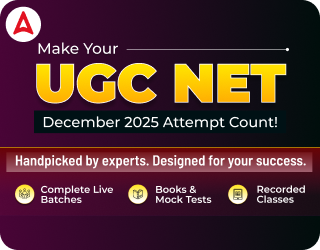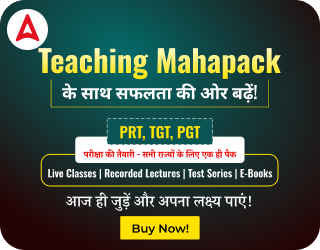Table of Contents
अव्यय परिभाषा, भेद और उदहारण : अव्यय (Avyay) is vast topic of Hindi Vyakaran. अव्यय topic contains types and its uses with examples. All the type of अव्यय has explained in this article. अव्यय topic contains many MCQ questions which come in TET exams. क्रिया विशेषण , सम्बन्ध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, निपात are explained for better preparation.
अव्यय ऐसे शब्द होते हैं जिनमें रूप परिवर्तन नहीं होता, चाहे वाक्य में उनका उपयोग किसी भी रूप में क्यों न किया जाए। ये शब्द स्थायी रूप से एक ही स्वरूप में रहते हैं और वाक्य में विभिन्न क्रियाओं, संज्ञाओं, विशेषणों आदि के साथ प्रयोग होते हैं। उदाहरणस्वरूप, “यहां,” “वहां,” “अब,” “तब,” “अतः,” “किंतु” आदि। अव्यय वाक्य को अधिक स्पष्ट और प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
अव्यय
अव्यय अविकारी शब्द है, जबकि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी शब्द हैं। उन शब्दों को अव्यय कहा जाता है जिनके रूप लिंग वचन, पुरूष, काल आदि के कारण परिवर्तित नहीं होते अर्थात् अपरिवर्तित रहते है। अव्यय का रूपान्तरण नहीं होता, इसी कारण इसे ‘अविकारी हैं-जब तब, किन्तु, परन्तु, इधर, उधर, अभी, अतएब, क्योंकि आदि।
अव्यय के भेद
अव्यय चार प्रकार के होते हैं-
- (क) क्रिया विशेषण
- (ख) सम्बन्ध बोधक अव्यय
- (ग) समुच्चय बोधक अव्यय
- (घ) विस्मयादि बोधक अव्यय
- (ड़) निपात
(क) क्रिया विशेषण
वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाते है,क्रिया विशेषण कहे जाते हैं। जैसे-
वह वहा टहलता है।
मैं इधर देखता हूँ।
जैसे: (i) साहिल रोज़ स्कूल जाता है। (रोज़’ शब्द ‘जाता है’ क्रिया की विशेषता उसका समय बतलाकर प्रकट करता है)
(ii) लड़का ज़ोर से चिल्लाता है। (ज़ोर’ शब्द ‘चिल्लाया’ क्रिया की विशेषता उसका ढंग बतलाकर प्रकट करता है)
(ii) चील ने नीचे देखा। (नीचे’ शब्द ‘देखा’ क्रिया की विशेषता उसका ढंग बतलाकर प्रकट करता है)
क्रिया विशेषण के भेद
क्रिया विशेषण के भेद– क्रियाविशेषण के भेद प्रयोग के अनुसार, रूप के अनुसार और अर्थ के अनुसार निम्न प्रकार किए जा सकते हैं-
| प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण | रूप के आधार पर क्रियाविशेषण | अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण |
|---|---|---|
| 1. साधारण क्रियाविशेषण अव्यय 2. संयोजक क्रियाविशेषण अव्यय 3. अनुबद्ध क्रियाविशेषण अव्यय |
1. मूल 2. यौगिक 3. स्थानीय |
1. कालवाचक क्रियाविशेषण अव्यय 2. स्थानवाचक क्रियाविशेषण अव्यय 3. परिमाणवाचक क्रियाविशेषण अव्यय 4. रीतिवाचक क्रियाविशेषण अव्यय 5. संख्यावाचक क्रियाविशेषण अव्यय 6. स्वीकारवाचक क्रियाविशेषण अव्यय 7. निषेधवाचक क्रियाविशेषण अव्यय 8. प्रश्नवाचक क्रियाविशेषण अव्यय |
अ. प्रयोग के अनुसार पर क्रियाविशेषण तीन प्रकार के होते हैं–
- साधारण क्रियाविशेषण अव्यय:- जिन शब्दों का प्रयोग वाक्यों में स्वतंत्र रूप से किया जाता है उन्हें साधारण क्रियाविशेषण अव्यय कहते हैं।
जैसे:
- हाय ! मै क्या करूँ।
- अरे ! वह साँप कहां गया ?
- संयोजक क्रियाविशेषण अव्यय:- जिन शब्दों का संबंध किसी उपवाक्य के साथ होता है उन्हें संयोजक क्रियाविशेषण अव्यय कहते हैं।
जैसे:
- जब अंकित ही नहीं तो मैं जी कर क्या करूंगी।
- जहाँ पर अब समुद्र है वहाँ पर कभी जंगल था।
- अनुबद्ध क्रियाविशेषण अव्यय:- जिन शब्दों का प्रयोग निश्चय के लिए किसी भी शब्द भेद के साथ किया जाता है उन्हें अनुबद्ध क्रियाविशेषण अव्यय कहते हैं।
जैसे:
- मैंने उसे देखा तक नहीं।
- आपके आने भर की देर है।
ब. रूप के अनुसार
रूप के अनुसार क्रिया विशेषण तीन प्रकार के बताए गए हैं-
- मूल:- जिन शब्दों में दूसरे शब्दों के मेल की जरूरत नहीं पडती उन्हें मूल क्रियाविशेषण अव्यय कहते हैं।
जैसे:
- अचानक से सांप आ गया।
- मैं अभी नही आया।
- यौगिक:- जो शब्द दूसरे शब्द में प्रत्यय या पद जोड़ने से बनते हैं उन्हें यौगिक क्रियाविशेषण अव्यय कहते हैं।
जैसे:
- तुम रातभर में आ जाना।
- वह चुपके से जा रहा था।
- स्थानीय:- वे अन्य शब्द भेद जो बिना किसी परिवर्तन के विशेष स्थान पर आते हैं उन्हें स्थानीय क्रियाविशेषण अव्यय कहते हैं।
जैसे:
- वह अपना सिर पड़ेगा।
- तुम दौडकर चलते हो।
अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण अव्यय के भेद
- कालवाचक क्रियाविशेषण अव्यय:– जिन अव्यय शब्दों से कार्य के व्यापार के होने का पता चले उसे कालवाचक क्रियाविशेषण अव्यय कहते हैं।
जहाँ पर आजकल , अभी , तुरंत , रातभर , दिन , भर , हर बार , कई बार , नित्य , कब , यदा , कदा, जब , तब, हमेशा , तभी , तत्काल , निरंतर , शीघ्र पूर्व , बाद , पीछे, घड़ी-घड़ी, अब , तत्पश्चात , तदनन्तर , कल , फिर , कभी , प्रतिदिन , दिनभर , आज , परसों , सायं , पहले , सदा , लगातार आदि आते है वहाँ पर कालवाचक क्रियाविशेषण अव्यय होता है।
- स्थान क्रियाविशेषण अव्यय: – जिन अव्यय शब्दों से कार्य के व्यापार के होने के स्थान का पता चले उन्हें स्थानवाचक क्रियाविशेषण अव्यय कहते हैं।
जहाँ पर यहाँ , वहाँ , भीतर , बाहर , इधर , उधर , दाएँ, बाएँ, कहाँ , किधर , जहाँ, पास , दूर , अन्यत्र , इस ओर , उस ओर , ऊपर , नीचे, सामने , आगे, पीछे , आमने आते है वहाँ पर स्थानवाचक क्रियाविशेषण अव्यय होता है।
- परिमाणवाचक क्रियाविशेषण अव्यय: – जिन अव्यय शब्दों से कार्य के व्यापार के परिणाम का पता चलता है उसे परिमाणवाचक क्रियाविशेषण अव्यय कहते हैं। जिन अव्यय शब्दों से नापतौल का पता चलता है।
जहाँ पर थोडा , काफी , ठीक , ठाक , बहुत , कम , अत्यंत , अतिशय , बहुधा , थोडा -थोडा , अधिक , अल्प , कुछ , पर्याप्त , प्रभूत , न्यून , बूंदबूंद, स्वल्प , केवल , प्राय:, अनुमानतः , सर्वथा , उतना , जितना , खूब , तेज , अति , जरा, कितना , बड़ा , भारी, अत्यंत , लगभग , बस , इतना , क्रमश: आदि आते हैं वहाँ पर परिमाणवाचक क्रियाविशेषण अव्यय कहते हैं।
- रीतिवाचक क्रियाविशेषण अव्यय: – जिन अव्यय शब्दों से कार्य के व्यापार की रीति या विधि का पता चलता है उन्हें रीतिवाचक क्रियाविशेषण अव्यय कहते हैं।
जहाँ पर ऐसे , वैसे , अचानक , इसलिए , कदाचित , यथासंभव , सहज , धीरे, सहसा , एकाएक , झटपट , आप ही, ध्यानपूर्वक , धडाधड , यथा , ठीक , सचमुच , अवश्य , वास्तव में , निस्संदेह , बेशक , शायद , संभव है , हाँ, सच, जरुर , जी, अतएव , क्योंकि , नहीं , न , मत , कभी नहीं , कदापि नहीं , फटाफट , शीघ्रता , भली-भांति , ऐसे , तेज, कैसे , ज्यों , त्यों आदि आते हैं वहाँ पर रीतिवाचक क्रियाविशेषण अव्यय कहते हैं।
- संख्यावाचक:– जिन शब्दों से क्रिया के होने की संख्या का ज्ञान हो। जैसे: मैं दो बार यह किताब पढ़ चुका हूँ।
- स्वीकार वाचक:– जिन शब्दों से क्रिया के होने की स्वीकृति प्रकट हो। जैसे: अच्छा, वह पास हो गया। हाँ, मैं तो जाऊँगा।
- निषेध वाचक:– जहाँ पर निषेध का भाव उत्पन्न हो।
- प्रश्नवाचक:- जहाँ पर प्रश्नसूचक शब्द व चिह्न का प्रयोग हो।
(ख) सम्बन्धबोधक अव्यय
जिन अव्वय शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम का वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ सम्बन्ध जाना जाता है, वे सम्बन्धबोधक अव्यय कहलाते हैं। अर्थ के अनुसार सम्बन्ध-बोधक अव्यय के ये भेद हैं-
- कालवाचक- पहले, बाद, ओग, पीछे।
- स्थानवाचक- बाहर, भीतर, बीच, ऊपर, नीचे।
- दिशावाचक- निकट पास, समीप, ओर, सामने।
- साधनवाचक- निमित्ति, द्वारा, जरिये।
- विरोधवाचक- उलटे, विरूद्ध, प्रतिकूल।
- व्यतिकवाचक- सिवा, अलावा, बिना, बगैर, अतिरित्त रहित।
- उद्देश्यवाचक- लिए, वास्ते, हेतु, निमित्त!
- साचर्यवाचक- समेत, संग, साथ, सहित।
- विशयवाचक- विषय, बाबत, लेख।
- संग्रहवाचक- समेत, भर, तक।
- विनिमयवाचक- प्लेट, बदले, जगह, एवज।
- सादृश्यवाचक- समान तरह, भाँति, नाई।।
- तुलनावाचक- अपेक्षा, वनस्पित, आगे सामने।
- कारणवाचक- कारण, पेरशानी से, मारे
प्रयोग की पुष्टि से संबंधबोधक अव्यय के भेद:
- सविभक्तिक:- जो अव्यय शब्द विभक्ति के साथ संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगते हैं उन्हें सविभक्तिक कहते हैं। जहाँ पर आगे, पीछे , समीप, दर , ओर, पहले आते हैं वहाँ पर सविभक्तिक होता है।
- निर्विभक्तिक:- जो शब्द विभक्ति के बिना संज्ञा के बाद प्रयोग होते हैं उन्हें निर्विभक्तिक कहते हैं। जहाँ पर भर, तक, समेत , पर्यन्त आते हैं वहाँ पर निर्विभक्तिक होता है।
- उभय विभक्ति:- जो अव्यय शब्द विभक्ति रहित और विभक्ति सहित दोनों प्रकार से आते हैं उन्हें उभय विभक्ति कहते हैं। जहाँ पर द्वारा , रहित , बिना , अनुसार आते हैं वहाँ पर उभय विभक्ति होता है।
क्रियाविशेषण और सम्बन्धबोधक अव्यय में अन्तर
जब इनका प्रयोग संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ होता है तब ये सम्बन्धबोधक अव्यय होते हैं और जब ये क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं तब क्रियाविशेषण होते हैं।
(ग) समुच्चयबोधक अव्यय
दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को मिलाने वाले अव्यय समुच्चबोधक अव्यय कहलाते हैं। इन्हें ‘योजक’ भी कहते हैं।
समुच्चयबोधक अव्यय तीन भेद है–
- संयोजक
जो अव्यय दो अथवा अधिक शब्दों या वाक्यों को जोड़ते हैं, वे संयोजक कहलाते हैं। जैसे-और, एवं, व आदि।
- मैं और राम काम पर जाएँगे।
- राम और लक्ष्मण तथा सीता ने पंचवटी में विश्राम किया।
इन दोनों वाक्यों में ‘और’, ‘तथा’ शब्द ‘जोड़ने’ के अर्थ में आए हैं, ये संयोजक है।
- विभाजक
जो अव्यय दो अथवा अधिक वस्तुओं में किसी एक का त्याग या ग्रहण बताते हैं, वे विभाजक कहलाते हैं। जैसे- किन्तु, परन्तु, अगर, ताकि, क्योंकि, इसलिए तथापि कि-तो आदि।
- करो या मरो
- नित्य आराम करो ताकि स्वस्थ रहो।
इस दोनों वाक्यों में ‘या’, ‘ताकि’ शब्द भेद प्रकट करते हुए जोड़ने के अर्थ में आए हैं। अतः ये विभाजक हैं।
- विकल्पसूचक
जो अव्ययविकल्प का बोध कराते हैं, ये विकल्पसूचक कहलाते हैं। जैसे-या, अन्यथा, अथवा, न कि, या-या इत्यादि।
- तुम आना या मैं आऊँगा।
- तुम पैसे का प्रबन्ध कर लो अन्यथा मुझे कुछ और करना पड़ेगा।
इन दोनों वाक्यों में ‘या’ और ‘अन्यथा’ शब्द आए हैं जोकि विकल्प का बोध करते हैं। अतः ये विकल्पसूचक हैं।
(घ) विस्मयादिबोधक अव्यय
जिन शब्दों से हर्ष, शोक, विस्मय, ग्लानि, घृणा, लज्जा आदि भाव प्रकट होते हैं, वे विस्मयादिबोधक अव्यय कहलाते हैं। उन्हें ‘द्योतक’ भी कहते हैं। प्रकट होने वाले भाव के आधार पर इसके निम्नलिखित भेद हैं-
- हर्षबोधक- अहा! धन्य!, वाह-वाह! ओह!, वाह!, शाबाश!
- शोकबोधक- आह!, हाय!, हाय-हाय!, हा, त्राहि-त्राहि बाप रे।
- विस्मयाबोधक- हैं! ऐं!, ओहो!, अरे, वाह!
- तिरस्कारबोधक- छिः।, हट!, धिक!, धत्!, छि छिः!, चुप!
- स्वीकृतिबोध- हाँ-हाँ!, अच्छा!, ठीक!, जी हाँ!, बहुत अच्छा!
- सम्बोधनबोधक- रे!, री!, अरे!, अरी!, ओ!, अजी!, हेला!,
- आशीर्वादबोधक- दीर्घायु हो!, जीते रहो!
(ड़) निपात
निश्चित शब्द, शब्द-अथवा पूरे वाक्य को अन्य भावार्थ प्रदान करने हेतु जिन शब्दों का प्रयोग होता है, उन्हें निपात कहते हैं। जो अव्यय किसी शब्द या पद के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष प्रकार का बल भर देते हैं, वे निपात या अवधारक अवयय कहलाते हैं।


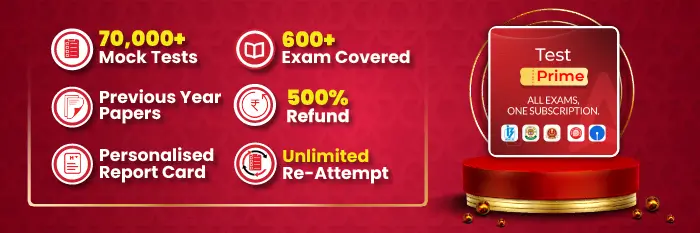
 Phases of Teaching - Stages of Teaching ...
Phases of Teaching - Stages of Teaching ...
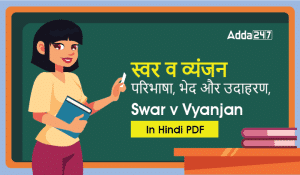 स्वर व व्यंजन - �...
स्वर व व्यंजन - �...
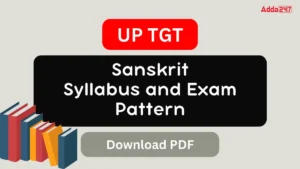 UP TGT Sanskrit Syllabus and Exam Patter...
UP TGT Sanskrit Syllabus and Exam Patter...